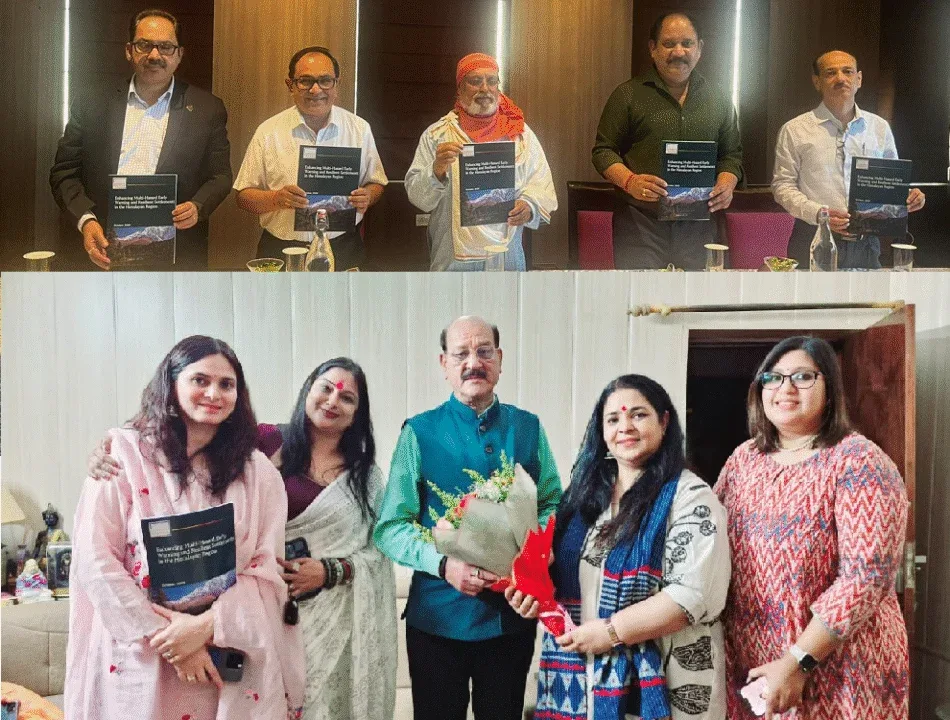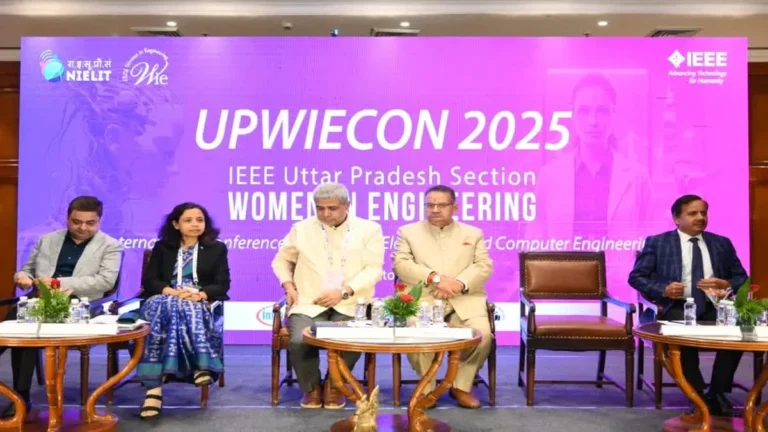एकीकृत हिमालयन एक्शन प्लान: जलवायु संकट के असर को कम करने के लिए मल्टी-हैजर्ड अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और सख्त भूमि उपयोग नियमों पर जोर
देहरादून, 15 अक्टूबर 2025 – एक नई रिपोर्ट “Enhancing Multi-hazard Early Warning and Resilient Settlements in the Himalayan Region” ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि हिमालय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जलवायु परिवर्तन और बेतरतीब मानव विकास ने अभूतपूर्व आपदा जोखिम पैदा कर दिए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि अब जरूरत है एक एकीकृत हिमालयन एक्शन प्लान की – जिसमें लोगों की भागीदारी हो, और पुराने, हदबद हो चुके आपदा प्रबंधन तरीकों की जगह एक ऐसा मल्टी-हैजर्ड वॉर्निंग सिस्टम बने जो सख्त भूमि उपयोग और आजीविका रणनीतियों से जुड़ा हो।
रिपोर्ट के विश्लेषण में सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघलते ग्लेशियर, बादल फटना और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) और भूस्खलन जैसे खतरे और गंभीर हो गए हैं। लेकिन असली चिंता यह है कि मानव गतिविधियां – जैसे बिना योजना के निर्माण और संवेदनशील इलाकों में बसावटों का विस्तार – इन प्राकृतिक खतरों को और बढ़ा रही हैं। नतीजा यह है कि जोखिम का चक्र लगातार मजबूत होता जा रहा है, और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मानवीय और आर्थिक नुकसान बढ़ने की आशंका है।
जापान, न्यूजीलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के उदाहरण लेते हुए रिपोर्ट ने हिमालयी क्षेत्र में “जीरो प्रिवेंटेबल डिसास्टर डेथ्स बाय 2030” यानी 2030 तक रोकी जा सकने वाली आपदाओं से होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य रखने की बात कही है। इसमें सुझाव दिया गया है कि तुरंत, कम लागत वाले रीयल-टाइम सेंसर (बारिश, मिट्टी की नमी और झील के जलस्तर के लिए) और मजबूत मोबाइल-आधारित अलर्ट सिस्टम लगाए जाएं, जिन्हें दीर्घकालिक सुधारों – जैसे जोखिम-संवेदनशील भूमि उपयोग योजना और योजनाबद्ध पुनर्वास – से जोड़ा जाए।
रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्य
रिपोर्ट के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- मल्टी-हैजर्ड अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (EWS) का ढांचा तैयार करना: एक ऐसा प्रणालीगत और लचीला चेतावनी तंत्र बनाना जो भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटना और GLOF जैसे विभिन्न खतरों से निपट सके। इसमें वास्तविक समय के मौसम, जलविज्ञान और भू-स्थानिक डेटा को स्थानीय समुदायों की प्रतिक्रिया प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
- जोखिम में कमी और सतत बसावट की योजना: उच्च जोखिम वाले इलाकों में बसावटों को नियंत्रित करने, भूमि उपयोग को संतुलित करने और योजनाबद्ध पुनर्वास को लागू करने की रणनीतियां सुझाना, ताकि खतरे का सामना घटे और शहरी व ग्रामीण विकास अधिक जलवायु-सक्षम बने।
- सामाजिक और आर्थिक लचीलापन बढ़ाना: ऐसे उपाय पहचानना जो जलवायु-संवेदनशील आजीविकाओं को मजबूत करें, पलायन का दबाव घटाएं और पर्वतीय समुदायों के लिए वैकल्पिक आय और रोजगार के अवसर बनाएं। लक्ष्य तात्कालिक अनुकूलन के साथ-साथ दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित करना है।
- व्यवहारिक बदलाव और मानसिकता में सुधार: हिमालयी आबादी, खासकर उत्तराखंड में, जोखिम को लेकर व्यवहारिक चुनौतियों का अध्ययन कर यह सुझाव देना कि कैसे लोगों में प्रोएक्टिव रिस्क परसेप्शन, नियंत्रण की भावना और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित की जाए। इसमें स्थानीय ज्ञान, सामुदायिक प्रशिक्षण और लक्षित व्यवहारिक संचार को शामिल करने की बात कही गई है, ताकि परिवार और समुदाय बेहतर तैयारियां करें और जलवायु कार्रवाई मजबूत हो।
- प्राकृतिक-आधारित समाधान (Nature-Based Solutions): जंगलों की बरकरार रखने, वाटरशेड प्रबंधन, एग्रोफॉरेस्ट्री, वेटलैंड संरक्षण और इकोसिस्टम-आधारित जोखिम न्यूनीकरण जैसे तरीकों को अपनाने की हिस्सेदारी की गई है। ये उपाय न केवल पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करेंगे, बल्कि मिट्टी और पानी की सुरक्षा, ढलानों की स्थिरता और आजीविका के अवसर भी बढ़ाएंगे।
- ज्ञान आदान-प्रदान और नीति एकीकरण: अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अपनाई गई सफल नीतियों और प्रथाओं का अध्ययन कर, उनसे सीखे गए सबकों को हिमालयी संदर्भ में लागू करने की बात कही गई है, ताकि नीति और योजना में ठोस, साक्ष्य-आधारित सुधार लाए जा सकें।
अंत में रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि इन सभी प्रयासों को जोड़ने के लिए एक “हिमालयन रेजिलिएंस फोरम” शुरू किया जाए, जो अगले दस सालों में चरणबद्ध तरीके से लागू हो। इसकी शुरुआत सबसे जोखिम वाले इलाकों में सेंसर लगाने और पायलट पुनर्वास योजनाओं से की जाए।
यह रिपोर्ट हिमालयी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश है, जो जलवायु संकट से निपटने में भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए रोडमैप प्रदान करती है।